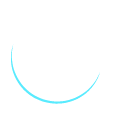नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2025 – आज जारी विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने की देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।
‘एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना’ शीर्षक वाले नवीन इंडिया कंट्री इकॉनोमिक मेमोरेंडम भारत में पाया गया है कि इस लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत की औसत 6.3 प्रतिशत* की तीव्र विकास दर मानते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पिछली उपलब्धियां इसकी भावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। तथापि, वहां तक पहुंचने के लिए सुधारों की आवश्यकता होगी और उनका कार्यान्वयन लक्ष्य के समान ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए।
विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि "चिली, कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से प्राप्त सबक यह दर्शाते हैं कि वे कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने एकीकरण को गहरा करके मध्यम-आय वाले देशों से उच्च-आय वाले देशों में सफलतापूर्वक परिवर्तित हुए हैं। इनका अनुसरण करके भारत सुधारों की गति को बढ़ाकर और अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपना रास्ता खुद बना सकता है।"
रिपोर्ट में अगले 22 वर्षों में भारत के विकास पथ के लिए तीन परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है। जिस परिदृश्य में भारत एक पीढ़ी में उच्च आय की स्थिति तक पहुंच सकता है, इसके लिए: क) सभी राज्यों में तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना; ख) वर्ष 2035 तक मौजूदा 33.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के कुल निवेश को बढ़ाकर 40 प्रतिशत (दोनों वास्तविक रूप में) करना; ग)समग्र श्रम शक्ति भागीदारी को 56.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत से ऊपर करना; और घ) समग्र उत्पादकता वृद्धि में तेज़ी लाना आवश्यक है ।
रिपोर्ट के सह-लेखक एमिलिया स्क्रोक और रंगीत घोष ने कहा कि "भारत मानव पूंजी में निवेश करते हुए, अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके और वर्ष 2047 तक महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को 35.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है।"
पिछले तीन वित्त वर्षों में भारत ने अपनी औसत वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर लिया है। इस गति को बनाए रखने और अगले दो दशकों में 7.8 प्रतिशत (वास्तविक रूप में) की औसत वृद्धि दर हासिल करने के लिए, कंट्री इकॉनोमिक मेमोरेंडम नीतिगत कार्रवाई के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सिफारिश करता है:
1. निवेश में वृद्धि करना: अधिक निजी और सार्वजनिक निवेश (वास्तविक निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 33.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 40 प्रतिशत करके) दीर्घकालिक विकास के लिए मूलाधार होगा। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के अधिनियम को मजबूत करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए औपचारिक ऋण की बाधाओं को दूर करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को सरल बनाने जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा ।
2. अधिक और बेहतर नौकरियां सृजित करने के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना: वियतनाम (73 प्रतिशत) और फिलीपींस (लगभग 60 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना भारत में कुल श्रम शक्ति भागीदारी दर कम (56.4 प्रतिशत) रही है। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को कृषि-प्रसंस्करण विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए लक्षित रणनीतियों, एक बृहद कुशल कार्यबल, वित्त तक अधिक पहुंच और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
3. बुनियादी ढ़ांचा परिवर्तन, व्यापार भागीदारी और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना: वर्तमान में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में भूमि, श्रम और पूंजी का आवंटन, फर्म और श्रम उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक को अपनाना, श्रम बाजार के नियमों को सुव्यवस्थित करना और फर्मों पर अनुपालन बोझ को कम करना उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा। ये कार्रवाई भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) भागीदारी दरों में थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे सहयोगी देशों की बराबरी करने में मदद करेंगी।
4. राज्यों को तेजी से और एक साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाना: रिपोर्ट में एक भिन्न नीति दृष्टिकोण अपनाने का तर्क दिया गया है, जिसके तहत कम विकसित राज्य विकास के मूल सिद्धांतों (स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, आदि) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि अधिक विकसित राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों (बेहतर कारोबारी परिवेश, जीवीसी में गहरी भागीदारी, आदि) को प्राथमिकता दे सकते हैं। केंद्र हाल ही में घोषित शहरी चुनौती निधि जैसे अधिक प्रोत्साहन-संचालित संघीय कार्यक्रमों के माध्यम से इस विकास प्रक्रिया को सुगम बना सकता है ताकि पिछड़े जिलों और राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सहायता की जा सके। अधिक प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण कम आय वाले राज्यों को सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करने और उन्हें अग्रणी राज्यों के साथ चलने में सक्षम बनाने में मदद करेगा।
*यदि हम वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 को छोड़ दें तो यह 6.6 प्रतिशत है, जो कोविड मंदी और तत्काल सुधार से प्रभावित था |